शिवताण्डवस्तोत्रम्
श्लोक ७
Shloka 7 Analysis![]()
करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्जवल-
द्धनंजयाहुतीकृतप्रचंडपंचसायके ।
धराधरेंद्रनंदिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ।।
| करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्जवल | → | करालभाल + पट्टिका + |
| धगद्धगद्धगद् + ज्वलत् | ||
| कराल | = | विकराल |
| भालपट्टिका | = | ललाटपट, मस्तकपट |
| धगद्धगद्धगद्ध | = | धधक धधक कर |
| ज्वलत् | = | जलती हुई |
| द्धनंजयाहुतीकृतप्रचंडपंचसायके | → | धनञ्जय + आहुतीकृत + |
| प्रचंड + पंचसायकः | ||
| धनञ्जय | = | अग्नि ने, अग्नि का एक नाम |
| आहुतीकृत | = | हवि बना दिया |
| प्रचंड | = | दुर्दम ,दुर्द्धर्ष |
| पंचसायकः | = | कामदेव, पंचशर |
| धराधरेंद्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक | ||
| धराधरेंद्रनन्दिनी | = | पर्वतराजपुत्री, पार्वती |
| कुचाग्र | = | वक्षस्थल का अग्रभाग |
| चित्रपत्रक | = | अंगों पर विविध प्रकार की चित्रकारी करना, पत्र -रचना करना |
| प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम | ||
| प्रकल्पनैक शिल्पिनि | = | चतुर चितेरे या सिद्धहस्त कलाकार में |
| त्रिलोचने | = | भगवन त्रिनयन में |
| रतिः + मम | = | रतिर्मम |
| रतिः | = | प्रीति, अनुराग |
| मम | = | मेरी |
![]()
अन्वय
कराल-भालपट्टिका धगद् धगद् धगद् ज्वलद् धनंजय आहुतीकृतं प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र – नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पने एकशिल्पिनि त्रिलोचने मम रति: ( भूयात् ) ।
भावार्थ
शिवजी के मस्तक पर धधकती हुई विकराल अग्नि ने दुर्द्धर्ष कामदेव को आहुति बना दिया । नगराज-नन्दिनी के वक्ष-कक्ष पर पत्रभंगी-रचना करने वाले अद्वितीय शिल्पी भगवान त्रिलोचन में मेरा अनुराग सदैव बना रहे ।
व्याख्या
शिवताण्डवस्तोत्रम् के सातवें श्लोक में स्तोत्रगायक रावण कहते हैं कि शिवजी के मस्तक पर धधकती हुई विकराल अग्नि में दुर्द्धर्ष पंचशर अर्थात् कामदेव हवि बन कर धू-धू कर जल उठे । धनंजय अर्थात् अग्नि ने प्रचण्ड कामदेव की आहुति ले ली । भगवान भाललोचन की भालाग्नि में वे तुरंत ही भस्मीभूत हो गये ।
 शंकर के ललाटपट से विनिःसृत धधकती हुई प्रचंड अग्नि कामदेव को देखते ही देखते लील गई । यह कथा सर्वविदित है कि कामदेव को तपोभंग के असाधु आचरण पर उद्यत देख कर क्रोधाविष्ट हुए शिव ने अपने भालस्थ तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिससे कालाग्नि की भांति धधकती हुई प्रचंड कराल ज्वाल निकली तथा दुर्दम, दुस्सह विषमविशिख (कामदेव के बाणों की संख्या पाँच होने के कारण उनको विषमविशिख भी कहते हैं ।) तत्क्षण वहीँ भस्मीभूत हो गये । विद्वान लेखक श्री सुदर्शन सिंह चक्र के अनुसार प्रलयंकर प्रभु तो स्वयं ही अग्निमात्र के परमोद्गम, परमाराध्य हैं । उनका तृतीय नेत्र ही अग्नि का वास्तविक आवास है । अग्निपुराण के अनुसार अग्निदेव सात जिव्हाओं से युक्त हैं, जिनके नाम हैं, कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नीललोहिता, सुवर्णा, पद्मरागा । श्री चक्र के अनुसार शास्त्रों ने मरुत् तथा अग्नि के उनचास-उनचास भेद किये हैं, किन्तु उन सभी का नाम केवल वैदिक महायज्ञों में ही स्मरण किया जाता है ।
शंकर के ललाटपट से विनिःसृत धधकती हुई प्रचंड अग्नि कामदेव को देखते ही देखते लील गई । यह कथा सर्वविदित है कि कामदेव को तपोभंग के असाधु आचरण पर उद्यत देख कर क्रोधाविष्ट हुए शिव ने अपने भालस्थ तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिससे कालाग्नि की भांति धधकती हुई प्रचंड कराल ज्वाल निकली तथा दुर्दम, दुस्सह विषमविशिख (कामदेव के बाणों की संख्या पाँच होने के कारण उनको विषमविशिख भी कहते हैं ।) तत्क्षण वहीँ भस्मीभूत हो गये । विद्वान लेखक श्री सुदर्शन सिंह चक्र के अनुसार प्रलयंकर प्रभु तो स्वयं ही अग्निमात्र के परमोद्गम, परमाराध्य हैं । उनका तृतीय नेत्र ही अग्नि का वास्तविक आवास है । अग्निपुराण के अनुसार अग्निदेव सात जिव्हाओं से युक्त हैं, जिनके नाम हैं, कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नीललोहिता, सुवर्णा, पद्मरागा । श्री चक्र के अनुसार शास्त्रों ने मरुत् तथा अग्नि के उनचास-उनचास भेद किये हैं, किन्तु उन सभी का नाम केवल वैदिक महायज्ञों में ही स्मरण किया जाता है ।
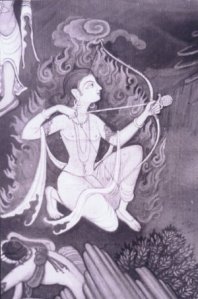 श्लोक में कराल शब्द अग्नि की भयंकरता का परिचायक है । कामदेव को प्रचण्ड पंचसायके कह कर रावण ने वस्तुत: मदन को दु:सह्य बताया है । सायक का अर्थ है बाण । उनके धनुष-बाण फूलों के हैं । उनके पंचबाणों के नाम हैं—अरविन्दमशोकं च आम्रं च नवमल्लिका, नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाणस्य सायका: । मदन के लिए कहा गया है कि स्मार्त पुष्पमयं चापं बाणा: पुष्पमया अपि । तथाप्यनंगस्त्रैलोक्यं करोति वशमात्मन: । अर्थात् स्मर (कामदेव) के शरचाप पुष्पमय हैं फिर भी अनंग (कामदेव) ने तीनों लोकों को अपने वश में किया हुआ है । सचमुच ही मनोज का मायाजाल दुर्भेद्य है । मदन की काम-कला की कादम्बरी का मद अन्ध और उन्मत्त करके रख देता है लोक में सभी को । हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ-चतुष्टय में तृतीय पुरुषार्थ के रूप में काम की गणना होती है । भारतीय आध्यात्मिकता काम को देवता की श्रेणी में रखती है न कि असुर की । वे कामासुर नहीं, कामदेव हैं । काम का संयत और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित आचरण प्रेम के उत्कर्ष में परिणत होता है, जो उसका उज्जवलतम पक्ष है । स्वामी अखंडानन्द सरस्वती ने विवाह संस्कार के विषय में कहा है, है तो यह पति-पत्नी का संबंध, परन्तु यह भोग से मुक्ति का तरीका है । विवाह भोग नहीं अपितु योग है । वर-वधू का संबंध आसक्ति में भक्ति है । उनके अनुसार स्वेच्छाचार या स्वच्छन्द आचरण में यह पवित्रता नहीं आ पाती है, किंतु विवाह-संस्कार के बंधन इसी प्रेम भावना का परिष्कार करके उसे उदात्त बना देते हैं । काम को अनंग, मनोज, मनोजव आदि मनपरक नामों से इसीलिए अभिहित किया गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मन में होती है । मन के उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट भावों से इसे वेष्टित कर मनुष्य सदाचारी या दुराचारी बनता है । क्षुद्र वासनाओं के गर्त्त में गिर कर गर्हित आचरण करने वाला प्रेमराज्य में विचरण करने का स्वत्व (अधिकार) खो बैठता है । शिव भाव को पुष्ट करने वाला काम पुरुषार्थ का स्थान पाता है । गौतम बुद्ध ने धम्मपद में मन के विषय में कहा है कि,
श्लोक में कराल शब्द अग्नि की भयंकरता का परिचायक है । कामदेव को प्रचण्ड पंचसायके कह कर रावण ने वस्तुत: मदन को दु:सह्य बताया है । सायक का अर्थ है बाण । उनके धनुष-बाण फूलों के हैं । उनके पंचबाणों के नाम हैं—अरविन्दमशोकं च आम्रं च नवमल्लिका, नीलोत्पलं च पंचैते पंचबाणस्य सायका: । मदन के लिए कहा गया है कि स्मार्त पुष्पमयं चापं बाणा: पुष्पमया अपि । तथाप्यनंगस्त्रैलोक्यं करोति वशमात्मन: । अर्थात् स्मर (कामदेव) के शरचाप पुष्पमय हैं फिर भी अनंग (कामदेव) ने तीनों लोकों को अपने वश में किया हुआ है । सचमुच ही मनोज का मायाजाल दुर्भेद्य है । मदन की काम-कला की कादम्बरी का मद अन्ध और उन्मत्त करके रख देता है लोक में सभी को । हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ-चतुष्टय में तृतीय पुरुषार्थ के रूप में काम की गणना होती है । भारतीय आध्यात्मिकता काम को देवता की श्रेणी में रखती है न कि असुर की । वे कामासुर नहीं, कामदेव हैं । काम का संयत और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित आचरण प्रेम के उत्कर्ष में परिणत होता है, जो उसका उज्जवलतम पक्ष है । स्वामी अखंडानन्द सरस्वती ने विवाह संस्कार के विषय में कहा है, है तो यह पति-पत्नी का संबंध, परन्तु यह भोग से मुक्ति का तरीका है । विवाह भोग नहीं अपितु योग है । वर-वधू का संबंध आसक्ति में भक्ति है । उनके अनुसार स्वेच्छाचार या स्वच्छन्द आचरण में यह पवित्रता नहीं आ पाती है, किंतु विवाह-संस्कार के बंधन इसी प्रेम भावना का परिष्कार करके उसे उदात्त बना देते हैं । काम को अनंग, मनोज, मनोजव आदि मनपरक नामों से इसीलिए अभिहित किया गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मन में होती है । मन के उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट भावों से इसे वेष्टित कर मनुष्य सदाचारी या दुराचारी बनता है । क्षुद्र वासनाओं के गर्त्त में गिर कर गर्हित आचरण करने वाला प्रेमराज्य में विचरण करने का स्वत्व (अधिकार) खो बैठता है । शिव भाव को पुष्ट करने वाला काम पुरुषार्थ का स्थान पाता है । गौतम बुद्ध ने धम्मपद में मन के विषय में कहा है कि,
मनसा ते पदट्ठेन भासती वा करोति वा
अर्थात् सभी धर्मों (कार्य-कलापों) का आरम्भ मन से है । मन श्रेष्ठ है । सारे कार्य मनोमय हैं । मन ऐन्द्रिक विषयों के प्रति अंधी आसक्ति छोड़ जब ईशचिंतन में निरत होता है तब वह अमृत का धारक हो जाता है ।
इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में रावण कहता है कि पर्वतराज पुत्री के वक्ष-प्रदेश का विविध प्रकार से पल्लव व पुष्प आदि से प्रीति-द्योतक श्रृंगार करने में पारंगत उन एकमात्र शिल्पी भगवान त्रिनयन में मेरी प्रीति सदा बनी रहे ।
 शिव-पार्वती का विलास-विहार निर्विकार है । इनका आमोद-प्रमोद इन्द्रियों का विषय नहीं है । इन नित्यदम्पति के पर्वत-विहार का स्मरण चिन्तन मन को विकारों से विमुख व विमुक्त करता है । और वहां एक पुण्य धारा प्रवाहित होने लगती है । यहां बताया गया है कि शिव अपनी लीलासंगिनी धरधरेन्द्रनन्दिनी का बड़ी निपुणता से श्रृंगार कर रहे हैं । रावण के वर्णन के अनुसार वे गिरिराजनंदिनि के कुचाग्र पर अर्थात् उरसिज (उरोज) के अग्रभाग पर तरुपत्रों एवं लाल-हरे किसलयों से अलंकरण कर रहे हैं , इसीको चित्रपत्रक कहा है । पुरातन समय में देह के अंग-प्रत्यंगों की सौंदर्य-वृद्धि के हेतु से, उन्हें अलंकृत करने के लिए उन पर चन्दन, केसर, मेहंदी, कदम्ब, रक्त-चंदन, कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्यों से चित्रकारी की जाती थी, बिंदियाँ और रेखाएं चित्रांकित की जाती थीं । इन्हें पत्रक, पत्रभंग, पत्रभंगी, चित्रपत्रक, पत्र-रचना तथा पत्रविशेषक आदि कहा जाता है । संस्कृत रचनाओं में तरु-पादपों, पर्वतों से प्राप्त इन श्रृंगारोपयोगी साधन द्रव्यों से स्त्रियों के समलंकृत होने का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है । बाणभट्ट की कादम्बरी में तो पत्र-रचना प्रसंगोल्लेख की बहुलता ध्यान खींचे बिना नहीं रहती । श्रृंगार तिलक, ऋतुसंहारं, रघुवंशं, कुमारसम्भवं आदि में भी उल्लेख मिलते हैं । एक उदाहरण कालिदास कृत कुमारसम्भवम् से प्रस्तुत है ।
शिव-पार्वती का विलास-विहार निर्विकार है । इनका आमोद-प्रमोद इन्द्रियों का विषय नहीं है । इन नित्यदम्पति के पर्वत-विहार का स्मरण चिन्तन मन को विकारों से विमुख व विमुक्त करता है । और वहां एक पुण्य धारा प्रवाहित होने लगती है । यहां बताया गया है कि शिव अपनी लीलासंगिनी धरधरेन्द्रनन्दिनी का बड़ी निपुणता से श्रृंगार कर रहे हैं । रावण के वर्णन के अनुसार वे गिरिराजनंदिनि के कुचाग्र पर अर्थात् उरसिज (उरोज) के अग्रभाग पर तरुपत्रों एवं लाल-हरे किसलयों से अलंकरण कर रहे हैं , इसीको चित्रपत्रक कहा है । पुरातन समय में देह के अंग-प्रत्यंगों की सौंदर्य-वृद्धि के हेतु से, उन्हें अलंकृत करने के लिए उन पर चन्दन, केसर, मेहंदी, कदम्ब, रक्त-चंदन, कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्यों से चित्रकारी की जाती थी, बिंदियाँ और रेखाएं चित्रांकित की जाती थीं । इन्हें पत्रक, पत्रभंग, पत्रभंगी, चित्रपत्रक, पत्र-रचना तथा पत्रविशेषक आदि कहा जाता है । संस्कृत रचनाओं में तरु-पादपों, पर्वतों से प्राप्त इन श्रृंगारोपयोगी साधन द्रव्यों से स्त्रियों के समलंकृत होने का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है । बाणभट्ट की कादम्बरी में तो पत्र-रचना प्रसंगोल्लेख की बहुलता ध्यान खींचे बिना नहीं रहती । श्रृंगार तिलक, ऋतुसंहारं, रघुवंशं, कुमारसम्भवं आदि में भी उल्लेख मिलते हैं । एक उदाहरण कालिदास कृत कुमारसम्भवम् से प्रस्तुत है ।
मापाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम्
स्वेदोद्गमः किम्पुरुषांगनानाम
चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु । (३३)
हिमालय पर्वत पर वसंत ऋतु में किन्नरियों की मुखछवि का वर्णन करते हुए कालिदास यहाँ कह रहे हैं  कि हिमपात के समाप्त हो जाने के कारण निर्मल ओष्ठ और कुछ श्वेत हुई मुख की कांति वाली किन्नर पत्नियों के मुख पर बनाई गई पत्र-रचना में स्वेद की बूंदों ने अपना स्थान बना लिया, अर्थात् उनकी पत्र-रचना में पसीने की बूँदें झलकने लगीं । अस्तु, इस श्लोक में गिरिजा के शतचन्द्रोज्ज्वल श्रीअंग पर महादेव द्वारा पत्र-रचना करना जहां उनके दाम्पत्य-जीवन के स्नेह-सौहार्द को संकेतित करता है, वहां यह चेष्टा शक्ति की प्रधानता की भी द्योतक है । उनके दिव्य दाम्पत्य जीवन की रस -माधुरी अनुपमेय है और उसका रस-रहस्य अननुमेय । शैलजा शिव की शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः भेद नहीं है। भगवान त्रिनयन पार्वती के प्राणवल्लभ ही नहीं उनके पुजारी भी हैं । अपने हाथों से उन्हें सजा कर प्रेम का परिपोषण करने वाले भगवान भाल-भूषण उनके वक्ष-कक्ष के चतुर चितेरे भी है । उनके स्नेह-सिक्त हाथों से पत्रभंगी पाकर पार्वती का श्रीशरीर चित्र-मन्दिर बन जाता है । किसी सिद्धहस्त कलाकार की भांति उमा के उर अथवा पयोधरतट पर पत्रभंग आदि उनके लीला-नाट्य हैं । वस्तुतः उनके इस श्रृंगार से युगल-तत्व की एकता लक्षित होती है । इसमें काम का संस्पर्श लेशमात्र भी नहीं है । काम तो स्वयं ही इन मायाधिप की माया से मोहित है । शिवपुराण में इस बात का उल्लेख है कि शिव की माया से विमोहित हो कर ही मदन ने इंद्र द्वारा निर्दिष्ट की गई शिव-तपोभंग की बात तुरंत मान ली थी ।
कि हिमपात के समाप्त हो जाने के कारण निर्मल ओष्ठ और कुछ श्वेत हुई मुख की कांति वाली किन्नर पत्नियों के मुख पर बनाई गई पत्र-रचना में स्वेद की बूंदों ने अपना स्थान बना लिया, अर्थात् उनकी पत्र-रचना में पसीने की बूँदें झलकने लगीं । अस्तु, इस श्लोक में गिरिजा के शतचन्द्रोज्ज्वल श्रीअंग पर महादेव द्वारा पत्र-रचना करना जहां उनके दाम्पत्य-जीवन के स्नेह-सौहार्द को संकेतित करता है, वहां यह चेष्टा शक्ति की प्रधानता की भी द्योतक है । उनके दिव्य दाम्पत्य जीवन की रस -माधुरी अनुपमेय है और उसका रस-रहस्य अननुमेय । शैलजा शिव की शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः भेद नहीं है। भगवान त्रिनयन पार्वती के प्राणवल्लभ ही नहीं उनके पुजारी भी हैं । अपने हाथों से उन्हें सजा कर प्रेम का परिपोषण करने वाले भगवान भाल-भूषण उनके वक्ष-कक्ष के चतुर चितेरे भी है । उनके स्नेह-सिक्त हाथों से पत्रभंगी पाकर पार्वती का श्रीशरीर चित्र-मन्दिर बन जाता है । किसी सिद्धहस्त कलाकार की भांति उमा के उर अथवा पयोधरतट पर पत्रभंग आदि उनके लीला-नाट्य हैं । वस्तुतः उनके इस श्रृंगार से युगल-तत्व की एकता लक्षित होती है । इसमें काम का संस्पर्श लेशमात्र भी नहीं है । काम तो स्वयं ही इन मायाधिप की माया से मोहित है । शिवपुराण में इस बात का उल्लेख है कि शिव की माया से विमोहित हो कर ही मदन ने इंद्र द्वारा निर्दिष्ट की गई शिव-तपोभंग की बात तुरंत मान ली थी ।
अग्रहीत्तरसा कामः शिवमायविमोहितः।
शिवमाया से मोहित काम यह न समझ पाया कि इनके तो चिंतन-मात्र से ही मोह-महिष का मर्दन होता है तथा मन विगत-कल्मष हो जाता है । शिव-शिवा का अलौकिक प्रेम व पवित्रतम संबंध वाणी का विषय नहीं । इनके तत्व के मर्म को तो वेदवेत्ता मुनि भी न जान पाये । शिव के प्रति रावण के उद्गार प्रेम-वारि से सिंचित हैं तथा भक्ति-क्षेत्र की अमूल्य निधि हैं । रावण ने परस्पर विरुद्ध भावों को उभारा है । एक ओर क्रोध की पराकाष्ठा है दूसरी और प्रेम का उत्कर्ष, जहाँ अनंग-व्यापार नहीं, सात्विकता का संचार है ।
लिंगपुराण कहता है कि शिव की गृहिणी दिव्य प्रकृति है । धराधरेन्द्रनन्दिनी प्रकारांतर से धरित्री ही हैं और धरती के उन्नत भाग अथवा उरःप्रदेश पर्वत हैं । प्रातः जागरण के समय भूमि-वंदना के श्लोक में पृथ्वी को पर्वतरूपी पयोधरों से मण्डलायित कहा गया है । वंदना इस प्रकार है,
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में ।
अतः पार्वती को सजाते हुए शिव प्रकारांतर से पर्वतराजपुत्री के साथ-साथ धरा को, प्रकृति को भी सजा रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐक्य है । उसमें वे चैतन्य फूंक रहे हैं । रावण उन्हें प्रकल्पनैक शिल्पी अर्थात् चतुर चित्रकार पुकारते हुए कहता है कि त्रिलोचने रतिर्मम अर्थात् ऐसे चतुर चितेरे व त्रिनयन में मेरी आसक्ति सदा बनी रहे, मेरी धारणा सतत और सदा उनके साथ लगी रहे । उनमें अनुरक्त और आसक्त होने का प्रीतिभाव मुझे गुदगुदाता रहे अर्थात् वे ही मेरे आनन्द के विषय हों । यह श्लोक भाव-राज्य की लोकोत्तर महिमा का चित्र उकेरता है ।
| पिछला श्लोक | अनुक्रमणिका | अगला श्लोक |
![]()

नमस्कार। ज्वलत् = जलाता हुआ। में ज्वलद् आएगा।
नमस्कार । मान्यवर, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया ।
नमस्कार। ज्वलद् धनंजय है मूल श्लोक में। ज्वलत् = जलती हुई ।क्या ज्वलद् और ज्वलत् का अर्थ समान है।
नमस्कार । जी हाँ, समान हैं । सन्धि के कारण त् का द् हुआ है ।